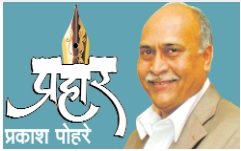
प्रकाश पोहरे, प्रधान संपादक, दैनिक ‘देशोन्नती’, हिंदी दैनिक ‘राष्ट्र प्रकाश’, साप्ताहिक ‘कृष्णकोणती’
किसी भी देश के आम नागरिक लोकतांत्रिक शासन को एक साधन के रूप में देखते हैं. उनके साध्य होते हैं-
- अपने जीवनस्तर को ऊपर उठाना
- दैनिक सुरक्षा,
- खुद के दुख-दर्द को कम करना
- उनके बच्चों की शिक्षा
- कम से कम अगली पीढ़ी को स्वाभिमान का जीवन मिलाने
- यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तो उसे समय पर उचित इलाज दिलाने
- बुढ़ापे में जब शरीर साथ न दे तो मेहनत न करने
- परिवहन सुविधाएं, बिजली, पानी आदि
ये अपेक्षाएं इतनी मानवीय और सार्वभौम हैं कि इसके लिए अलग से सर्वे करने की जरूरत नहीं है! लेकिन मुख्यधारा के थिंक टैंक और पूंजीवाद समर्थक विचारक भी यह मानने लगे हैं कि पिछले 40 वर्षों में, दुनिया भर के अरबों आम नागरिकों की वित्तीय स्थिति आग की लपटों में घिर गई है.
इसके कारणों को निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक दर्शन में खोजना होगा. यह वर्तमान में हमारे भारत की बड़ी पीड़ा है.
हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा-
- एलआईसी
- जीआईसी (सामान्य बीमा निगम)
- गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)
- भेल
- आईडीबीआई
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- राजमार्ग
- गोदाम
- एयरपोर्ट
- एयर इंडिया
- पवन हंस
- इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन
- रेलवे
- स्टेडियम
- इंडियन ऑयल की पाइपलाइन…
जैसी कई गतिविधियां निजी कंपनियों को सौंप दी गईं हैं.
वैसे तो 1991 से ही केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है. केवल इस बार एक बड़ा कदम उठाया गया है. ये सभी कंपनियां जनता के टैक्स के पैसे से बनाई जाती हैं.
हम रिक्शावाले को दो रुपए नहीं छोड़ते, सब्जी वाले से तीन-चार रुपए के लिए बहस करते हैं. लेकिन जो सरकार हर चीज पर टैक्स लगाती है, हम उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते. हमें इसे भारत के नागरिक के तौर पर बदलना होगा.
सरकार सभी घरेलू और विदेशी कंपनियों के माध्यम से इस विशाल उद्योग का निर्माण करना चाहती है, लेकिन सरकार आम लोगों के कल्याण की गारंटी नहीं दे सकती. हमारे देश पर सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक का कर्ज है. फिर भी हम ‘आत्मनिर्भरता’ का डंका बजा रहे हैं, विदेशी कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं. इससे बड़ी दूसरी कोई शोकांतिका नहीं है. यानी एक परिवार ने अपनी जमीन बेच दी, अपने घर का सामान बेच दिया, अब घर की छत बिक्री के लिए निकल दी गई हैं, फिर भी घर के सामने ‘आत्मनिर्भरता’ का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है. ऐसे परिवार को समाज पागल घोषित कर मानसिक अस्पताल भेज देता है, लेकिन केंद्र सरकार यही कर रही है, फिर भी उसकी ‘प्रशंसा’ हो रही है. यही हमारी आर्थिक अज्ञानता है.
भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारणों को आगे बढ़ाकर देश को समाज और राष्ट्र की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के निजीकरण की ओर ले जाना एक गंभीर मामला है. मुद्दा सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण तक ही सीमित नहीं है. इन प्रकारों के बीच एक पैटर्न उभर कर आता है. सरकार अपील कर रही है कि देशी-विदेशी कंपनियों, हमने अपनी सरकारी कंपनियों को औने-पौने दामों पर बेचने निकाला है, उनकी नीलामी शुरू कर दी है, आपके लिए श्रम कानून बदल दिए हैं, कंपनी टैक्स कम कर दिया है. तो आप आएं और हमारे बाजार पर कब्जा करें, और इसे ही ‘मेक इन इंडिया’ कहा जाता है.
जब देश बेचने निकाला गया है, तब सरकार को ‘आत्मनिर्भरता’ की याद आयी है. वास्तव में यह नारा एक बड़े कद्दू की तरह है, जिसके अंदर खोखलापन है!
वैश्वीकरण के आर्थिक दर्शन में जो सबसे जोरदार हल्ला मचाया गया है, वह शासन की अर्थव्यवस्था के मामले में. अस्सी के दशक तक यह माना जाता था कि सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करेगी, कि सरकार औद्योगिक पूंजीवाद के कुछ वर्षों के बाद नियमित रूप से होने वाली मंदी जैसी स्थितियों में रोजगार पैदा करने के लिए हस्तक्षेप करेगी, और वह यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यम चलाएगी, जहां बाजार की ताकतें माल और सेवाओं की आपूर्ति करने में असमर्थ थीं. लेकिन, वैश्वीकरण के पीछे नवउदारवाद ने देश की अर्थव्यवस्था से सरकार को वापस लेने का अत्यधिक आग्रह किया और इसे लागू किया. इस चक्की में भारत के आम नागरिक बहुत ही खराब तरीके से पिसे जा रहे हैं.
निजीकरण क्या है?
निजीकरण गुलामी का ऐसा एक फंदा है, जो धीरे-धीरे आपका गला घोंट देगा! निजीकरण पहले सरकारी दफ्तरों-उद्योगों को बदनाम करता है.
बीएसएनएल का उदाहरण याद करें. कहीं रेंज नहीं, कभी कॉल ड्रॉप आदि की समस्या होने लगी थी. फिर निजीकरण के पैरोकार, सरकार के माध्यम से ही शासन के स्वामित्व वाले उद्यमों को बंद करवाते हैं. बाद में वे उन्हीं उद्योगों को औने-पौने दामों में खरीदते हैं और ‘दुनिया मुट्ठी में’ के रूप में व्यापार करते हैं. अब रेंज नहीं होती या कॉल कट जाती है या बिल ज्यादा हो तो भी चर्चा नहीं होती! यह दांवपेंच नोट कर लें!!
अब नजर शिक्षाक्षेत्र पर! आपने और हमने जिला परिषद या नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाई की है. भले ही वह कम ही क्यों न रही हों, तब स्कॉलरशिप और फीस में छूट मिलती थी. अब यह सब बंद हो रहा है. सरकार ने स्कूलों को खोलना ही बंद कर दिया है. सरकार कह रही है कि निजी उद्योगपति आकर स्कूल-कॉलेज-यूनिवर्सिटी बनाएं. वहां बहुत फीस होगी, जो आप वहन नहीं कर सकते. साथ ही न फीस माफी, न छात्रवृत्ति। तो फिर आप सीखेंगे कैसे?
वैसे ही सरकारी अस्पताल भी हैं! पहले सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज-दवाइयां मिलती थीं. अब वहां भी बाहर से दवाइयां मंगवाई जाती हैं, बाहर से एक्स-रे लिए जाते हैं, बाहर से टेस्ट होते हैं. सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. सरकार निजी क्लीनिकों को बढ़ावा दे रही है. आप वहां महंगा इलाज नहीं करा सकते. तो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप अपने हाथ-पैर गंवाकर मर जाएंगे? उसके समाधान के रूप में, निजी चिकित्सा बीमा कंपनियां आईं और अब इससे बहुत से लोगों ने बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का अनुभव किया है.
शिक्षा, स्वास्थ्य, बीज, बिजली, पानी और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजों का कभी भी व्यावसायीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में देश इसी पर खड़ा है, लेकिन जब ये सारी चीजें निजी निवेशकों वाली कंपनियों या पूंजीपतियों को सौंप दी जाएंगी, तो देश का क्या होगा! यह बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है.
कुछ लोग कहते हैं कि निजीकरण अच्छा है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है. उन्हें गलतफहमी है कि प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार नहीं है! सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र में 100 गुना अधिक भ्रष्टाचार है. यह सिर्फ इतना है कि नागरिक इससे संबंधित नहीं हैं, इसलिए वे इसे नहीं जानते हैं और इसे नहीं देख पाते हैं. निजी क्षेत्र के टेंडरों में, कच्चा माल लाने में, नियुक्तियाँ करने आदि मामलों में बहुत लेन-देन होता है! आम नागरिक इस आदान-प्रदान को समझ नहीं पाते हैं. इसलिए, उन्हें यह खुशफहमी-ग़लतफ़हमी है कि निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त है.
निजी कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को इस तरह से निर्धारित करती हैं कि सभी लागतों की वसूली हो जाए और कोई भी सामान और सेवाएं प्रदान करते समय लाभ भी कमाया जाए. लेकिन कई वस्तुएं, सामान और सेवाएं जैसे– पानी, बिजली, सीवेज, सड़क, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सेवाओं को आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उनकी कीमतें नागरिकों की जेब के लिए अवहनीय हो जाती हैं, जिससे उनके जीवन स्तर पर असर पड़ता है. आने वाली पीढ़ियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और सामाजिक और राजनीतिक असंतोष खदबदाने लगता है. ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें सामाजिक प्रतिफल वित्तीय प्रतिफल से अधिक है. भारत जैसे असमान रूप से विकसित देश में अविकसित क्षेत्रों का विकास केवल और केवल सार्वजनिक उद्यम स्थापित करके ही किया जा सकता है. यह इस कारण से है कि कई शताब्दियों के लिए दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उपर्युक्त सामान और सेवाएं प्रदान की गईं. इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि नवउदारवाद ने सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है. इसने देश में मौजूद कई सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है, और अभी भी किया जा रहा है और इससे सरकार द्वारा नए सार्वजनिक उद्यमों का निर्माण हुआ है.
तो वह समय दूर नहीं, जब इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि ये भारत का आखिरी सरकारी स्कूल, आखिरी सरकारी ट्रेन, आखिरी सरकारी बस, आखिरी सरकारी बिजली कंपनी, आखिरी सरकारी हवाई अड्डा और आखिरी सार्वजनिक उद्योग था! यदि किसी सरकारी उपक्रम या सरकारी संस्थान का निजीकरण किया जाता है, तो आम लोगों की चुप्पी की कीमत एक दिन पूरे देश को चुकानी पड़ेगी! क्योंकि जब सारे स्कूल, सारे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बिजली, पानी, बीज, बस सेवा सब निजी हाथों में है! याद रखें कि सरकार और सरकारी उपक्रमों का लक्ष्य न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना होता है, जबकि निजी संगठनों का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाना होता है.
नवउदारवादी आर्थिक दर्शन की पूंजीवादी संकीर्णता अब दुनिया भर में व्यापक रूप से उजागर हो गई है. कई मुख्यधारा के अर्थशास्त्री, जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, ने नवउदारवाद की ज्यादतियों का उपहास करना शुरू कर दिया है. वे लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं कि नवउदारवाद दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक असमानता, राजकोषीय (आवर्ती आपदाओं), पर्यावरण (कार्बन उत्सर्जन) के मुद्दों से जुड़ा है.
पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए निजीकरण की साजिश पर देश की जनता का चुप रहने का मतलब अपनी गुलामी के फंदे को अपने ही हाथों से मजबूत करना ही है! क्योंकि मुसीबत के समय सिर्फ सरकारी विभाग ही काम आते हैं, कोई निजी विभाग काम नहीं करता, जैसा कि आपने हाल ही में एक उदाहरण देखा होगा. कितने निजी अस्पताल कोविड के दौरान मुफ्त या न्यूनतम लागत में इलाज कर रहे थे? कितनी निजी बसें मजदूरों, कामगारों और छात्रों को लेकर जा रही थीं? कितने निजी संगठन और एनजीओ जमीन पर जनता की मदद कर रहे थे? कोविड काल में कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस भारतीयों को फ्री एयरलिफ्ट नहीं दे रही थी!
हालाँकि, राजनीतिक शक्ति केवल एक आभास है. व्यवसायी तय करता है कि इसे कितना सजाना है. ऐसे में सरकार ने दिन-ब-दिन निजीकरण का दायरा बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था से पीछे हटने का आसान रास्ता चुना है. इसलिए इसका विरोध होना ही चाहिए, नहीं तो भविष्य में इस देश को चंद उद्योगपति ही चलाएंगे और गुलामी का दौर भारत में पहले की तरह लौट आएगा. सत्ता और मूल्यवान संपत्तियां केवल मुट्ठीभर लोगों के हाथों में होगी! तो अब यह तय करने का समय आ गया है कि हम अपने आप को बचाने के लिए क्या योगदान देने जा रहे हैं? भले ही बहुत देर हो चुकी हो..!

