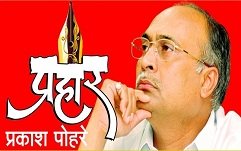
लोकतंत्र एक वैचारिक ढाँचा है, उस ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने के बाद आम चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से न केवल केंद्र, बल्कि पंचायतों और स्थानीय स्व-सरकारी निकायों को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया। लोकतंत्र एक पेड़ की तरह है। पेड़ की जड़ें मिट्टी में जितनी गहराई तक जाती हैं, पेड़ उतना ही अधिक छायादार हो जाता है। 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद, आदर्श यह था कि आयोग ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बरकरार रखते हुए ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, कई विधान सभा और लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए, लेकिन अब ‘एक देश, एक चुनाव’ का आकर्षक लेकिन भ्रामक नारा प्रचलन में है, यह कपटपूर्ण है। क्योंकि अब भी पूरे देश में एक ही चुनाव होता है – लोकसभा का, तो इसकी घोषणा करने की क्या जरूरत थी?
अब सभी चुनाव वास्तव में कौन-कौनसे हैं? हम आशा करें कि प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक आम रुख यह होना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। यदि इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका और नगर निगम की अपेक्षा की जाए, तो उलझन और अधिक हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है, हर राज्य का चुनाव कार्यक्रम अलग-अलग होता है, तो फिर जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, क्या वहां भी विधानसभाएं भंग कर दी जायेंगी? फिर तोयह तानाशाही हो गई।
देश में लोकसभा, प्रदेश में विधानसभा की तरह ही गांवों में ग्राम सभाएं और शहरों में प्रभाग हैं। ये ग्राम सभाएँ स्वायत्त हैं, ऐसी ग्राम सभाएँ राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना की मूल इकाई होती हैं। इसके बाद स्थानीय स्व-सरकारी निकाय आते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के सामने चुनौती नियमित रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराने, मुद्दों का समाधान करने और खुद को एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित करने की है। इसका कारण यह है कि अब हमारे राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कुछ दिखावटी कारण दिखाकर स्थगित कर दिये गये हैं। वहीं, देश में अगले 2024 लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र का विपरीत चक्र चल रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से सभी चुनाव एक साथ कराने का विचार रखा। तब से, चुनाव कितने महंगे हैं और वे सरकार की नीतियों को कैसे कमजोर करते हैं, इसकी शिकायतें लगातार आती रही हैं। कुछ भाजपा-शासित राज्यों के प्रतिभाशाली(?) मुख्यमंत्री इसमें और भी जोड़-जुगाड़ कर रहे हैं और इसे ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव एक ही दिन कराने के महाकाव्य तक ले जा रहे हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 3426 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अगर कोई यह आंकड़ा हमारे सामने उछाल दे, तो हम निश्चित रूप से भयभीत हो जाएंगे, लेकिन जब हम इतनी बड़ी संख्या को देखते हैं, अगर हम यह देखना शुरू करते हैं कि प्रति मतदाता कितना खर्च किया जाता है, तो हम क्या देखते हैं? 2014 में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रति मतदाता लागत लगभग 42 रुपये थी – और वह भी कुल पांच वर्षों के बाद! तो, 2014 के बजट में एक वर्ष के लिए कुल 17,94,892 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। उस पृष्ठभूमि में, अब से पाँच साल बाद (और उससे भी पहले) चुनाव की लागत पर कितनी चर्चा की जाए?
इसके अलावा केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होने पर भी बैलेट पेपर और पेपर ट्रायल का खर्च अलग से करना होगा। केवल सुरक्षा बलों और वास्तविक चुनाव कर्मचारियों पर होने वाले खर्च से बचा लिया जाएगा। इसलिए लागत का मुद्दा दांत निकालने और खिलाने का मामला है। असल मसला तो यह है कि अब केंद्र के सत्ताधारियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वे यह महसूस करने में विफल रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आम आदमी अब केंद्र सरकार से परेशान है। उन्होंने इसका समाधान निकाला, वह है ‘एक देश, एक चुनाव’! इसके तहत सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इस प्रकार की तुगलकी हरकत करके लोकतंत्र के चक्र को उल्टा कर दिया गया और संविधान को नष्ट कर संसदीय प्रणाली में हेरफेर किया गया। फिर वही बात…प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता बढ़ाने का ढोल पीटते थे…मोदी ने 2014 के ‘अच्छे दिन’ और विकास के एजेंडे को साबरमती नदी में छोड़ दिया है। अब वे पाकिस्तान, हिंदू-मुसलमान, राम मंदिर के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मोदी यह प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे कि उन्होंने देश के विकास के लिए सत्ता छोड़कर कितना त्याग किया है, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है!
जब हमें एहसास होता है कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे वोट कम हो रहे हैं, तो हमें समय से पहले चुनाव करा लेना चाहिए और जितना हो सके नुकसान से बचना चाहिए। विकास, सत्ता त्याग आदि की आड़ में प्रचार-प्रसार में भारी पैसा बहाकर इस पर पर्दा डाला जाएगा!!
यदि यह झूठ है और भाजपा वास्तव में एक के बाद एक चुनावों को विकास में बाधा के रूप में देखती है, तो पांच राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराते? यानी लोग समझ गए होंगे कि सत्ता का मोह है या नहीं! खैर….
इस सत्तारूढ़ कारक से परे एक साथ चुनाव कराने के मुद्दों में एक गंभीर व्यापक राजनीति है। यह देश में जबरन चुनाव कराकर और प्रचार का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की एक चाल है जो उन राज्यों के मुद्दों को कवर कर लेगी। भारत एक संघीय राज्य है। उनमें से प्रत्येक राज्य के कुछ प्रश्न हैं। अपने-अपने चुनाव में उन सवालों पर चर्चा होती है। लोग इस पर सोचते हैं और अपनी राय देते हैं। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार प्रशासन के स्तर पर बुरी तरह विफल रही है, लेकिन मोदी देश के चुनाव प्रचार में कुछ ऐसे मुद्दे लाएंगे कि राज्य की ये समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। यह लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश है। एक तरह से, मोदी ने इस संसदीय संघीय राज्य को अध्यक्षीय (राष्ट्रपति) शासन प्रणाली में बदलने के लिए मंच तैयार कर दिया है। मूलतः यही विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। संघ से होने के कारण ही मोदी उन विचारों को अमल में ला रहे हैं।
भारत ने संसदीय लोकतंत्र क्यों अपनाया? अनेक लोगों को एक साथ शासन क्यों करना चाहिए? इसलिए यहां कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। निर्णय-प्रक्रिया में उन्हें स्थान मिलने से उनके हित एवं पहचान भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहां सरपंच और मेयर का चुनाव सीधे होता है। एक बार जब यह ‘एक देश, एक चुनाव’ मॉडल स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऊपर से नीचे तक सीधे नेताओं को चुनने की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली शुरू की जाएगी और यह यहां के संसदीय लोकतंत्र के लिए चुनौती पैदा करेगा।
आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के तात्कालिक लक्ष्य और भविष्य में देश को केंद्रीकृत सत्ता और अधिनायकवाद की ओर ले जाने के दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ‘एक देश, एक चुनाव’ नामक यह मंच तैयार किया जा रहा है। एक तरफ मीडिया, पुलिस व्यवस्था, चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता के मद में चूर हैं, वहीं तानाशाही रवैया सीधे सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठ कर चुका है, अब यह नया मुद्दा जबरदस्ती सामने लाया जा रहा है। यह एक ऐसी तरकीब है, जो देखने में शानदार लगती है, लेकिन वास्तव में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि यहां की संघीय व्यवस्था को बचाने के लिए उसे सफल होने दें या शुरू से ही उसका विरोध करें।
2014 में जिसने भी कहा था कि लोग संविधान बदलकर ‘मनुस्मृति’ लाने के बारे में सोच सकते हैं, क्या तब किसी ने उन पर विश्वास किया था? छह माह पहले होना चाहिए चुनाव, ऐसी राजनीति पहले भी कई नेता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेई समय से पहले लोकसभा चुनाव करा चुके हैं। लेकिन उनका उद्देश्य इतना भी टेढ़ा नहीं था। लेकिन ये वो दिन नहीं हैं। ये दिन अलग हैं। अभी तो सीधा कुछ हो ही नहीं रहा है!!
संभवतः इस प्रस्ताव को लागू होने में काफी समय लग सकता है, लेकिन जिस जिद के साथ सरकार इस पर चर्चा करा रही है, उसे देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि हमारी संसदीय प्रणाली के बारे में संविधान के मूल ढांचे में व्यवस्थित रूप से भ्रम पैदा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं!
—————————–
लेखक : प्रकाश पोहरे
(संपादक- दैनिक देशोन्नति, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति)
संपर्क : 98225 93921
2prakashpohare@gmail.com

