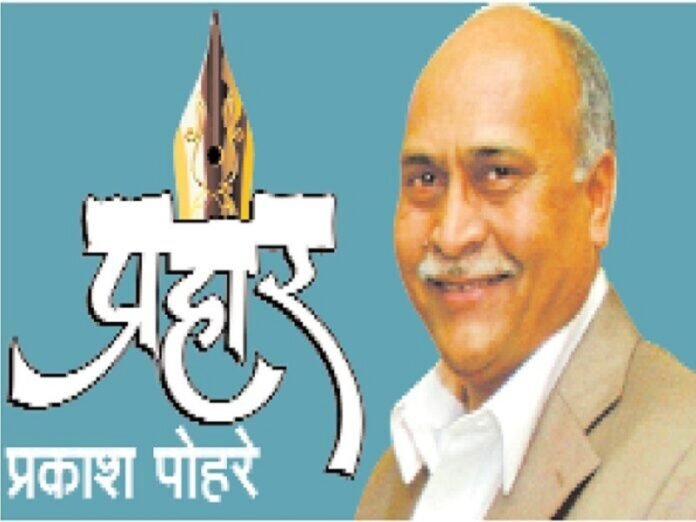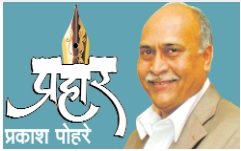
शहरों के नाम बदलने को लेकर इस समय महाराष्ट्र और देश भर में विवाद चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में, साम्राज्यवादी अंग्रेजों के प्रतीकों और नामों को शांतिपूर्ण तरीके से बदल दिया गया। देश में इस पर कोई विवाद नहीं था। यह स्वतंत्र भारत का नया प्रतीक था। हालांकि, हाल में हुए नाम परिवर्तन में धार्मिक पहचान का रंग साफ नजर आता है। सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी यही चाहता है। बेशक, सत्ता पक्ष जो चाहता है, विपक्ष नेक नीयत से करता दिख रहा है।
जैसे स्वराज्य के इतिहास का एक पात्र औरंगजेब वर्तमान में अचानक कब्र से बाहर लाया गया है और पूरे राज्य में एक अनावश्यक चर्चा शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष इस चर्चा को हवा दे रहा है।
वास्तव में हमारे देश में एक स्थान, एक गांव, एक सड़क हमारे ही प्रेरक महापुरुषों के नाम से सुशोभित है। फिर भी अगर कोई ऐसे नाम देने के खिलाफ है, तो कानूनी तौर पर उसकी भड़ास निकालनी चाहिए। हमारे महापुरुषों के नाम का विरोध करने वालों पर शासन करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि, यहां मामला कुछ अलग है। जैसा कि अब कई वर्षों के बाद औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजीनगर’ कर दिया गया और एमआईएम पार्टी के एक सांसद ने इसका विरोध किया। देखा जा रहा है कि ये सांसद औरंगजेब के नाम पर अटका हुआ है।
मूल रूप से ऐसे विरोध से शासकों को ही लाभ होता है। क्योंकि, जब कोई विषय सत्ताधारियों द्वारा आगे लाया जाता है, तो उसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए, यह पहले से ही नियोजित होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा ऐसे मुद्दों को आगे लाया जाता है, तो एक ‘बी टीम’ जानबूझ कर इसका विरोध करने का नाटक करने को तैयार हो जाती है, ताकि धार्मिक पहचान रंग में आ सके और उसकी राजनीतिक पूंजी बनाई जा सके!
यहां विशेष उल्लेखनीय है कि ऐसी ‘बी टीम’ के नेताओं पर ईडी, सीबीआई के छापे कभी नहीं पड़ते! औरंगाबाद का नाम बदलने से भी उसी राजनीति की बू आ रही है। वास्तव में शहरों के नाम बदलने के सरकार के अधिकार को कोई नकार नहीं सकता। नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखें कि शहरों के नाम बदलना केवल सरकार का मुख्य काम नहीं है। लोक कल्याण करना, विकास प्राप्त करना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना और सबसे महत्वपूर्ण कृषि और किसानों की समस्याएँ भी सरकारों के मुख्य कार्य हैं।
हम आज ऐसे देश में जी रहे हैं, जहां अतीत से मोहभंग हो चुका है। वर्तमान को लेकर अत्यधिक असंतोष है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का भाव है। यह बहुत ही अस्थिर अवधि है और बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसे समय में शासक अक्सर अपनी नाकामी और लोगों में असुरक्षा की भावना को छिपाने के लिए किसी को दोष देने की सोचते हैं और ऐसे में विदेशियों पर आरोप लगाना या साम्प्रदायिक प्रचार करना सबसे आसान तरीका है। आज लोगों की इस भावना का लाभ असहिष्णु, राष्ट्रवाद से प्रेरित आंदोलनों और विचारधाराओं को ही मिलता है। ऐसे समय में मिट्टी में जाने वाले भी नहीं जानते कि हम मिट्टी में जा रहे हैं!
अब आइए देखते हैं महाराष्ट्र के मौजूदा हालात! 42 लाख हेक्टेयर या लगभग एक करोड़ एकड़ क्षेत्र में उगाए गए 60-70 लाख किसानों की कपास को दो महीने तक घर पर रखने की नौबत किसानों पर आ गयी है। व्यापारियों और सरकार के बीच ये किसान फंसे हुए हैं। कपास का भाव नहीं मिलने से पिछले दो माह में ही 136 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जब भाव नहीं मिला, तो खर्चा नहीं निकल पाएगा और कर्ज की अदायगी तथा अगली फसल कैसे पूरी होगी।
स्वराज्य के दुश्मन औरंगजेब को अचानक कब्र से बाहर लाने वाले और अनावश्यक हंगामा करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि आज राज्य में दो-तीन किसान और देश में प्रतिदिन 12 किसान, उसमें भी विदर्भ और मराठवाड़ा में अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
2022 के एक कैलेंडर वर्ष में, महाराष्ट्र में 2942 किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं, यानी प्रति दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि इस वर्ष विदर्भ में ही 1322 किसानों ने आत्महत्या की है। 2001 से 2022 तक विदर्भ में 21,084 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। इनमें से 75 प्रतिशत किसान थे, जिन पर बैंक ऋण के रूप में केवल 40,000 से 50,000 रुपये थे। 2019 से 2022 तक चार साल में मराठवाड़ा में भी 3443 किसानों ने आत्महत्या की।
हालांकि, सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कपास की गांठों के आयात का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और राज्य के पास इसका विरोध करने का साहस और ताकत नहीं है। आयात के कारण कपास के दाम गिर रहे हैं। पिछले दिसंबर में केंद्र सरकार ने 11 फीसदी टैक्स माफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया से तीन लाख गांठ कपास (51 हजार टन कपास) आयात करने का फैसला किया था। इससे घरेलू स्तर पर उत्पादित कपास की कीमतों में गिरावट आई है।
फिलहाल प्याज की कटाई का सीजन खत्म हो चुका है। किसान प्याज के अच्छे बाजार मूल्य की उम्मीद कर रहे थे। प्याज की उत्पादन लागत प्रति एकड़ पचास हजार तक है। हालांकि उपज 65 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। प्याज का वर्तमान बाजार भाव 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल है। यानी प्याज की बिक्री से उत्पादन लागत तो निकलती नहीं, बल्कि किसान के पसीने (मेहनत) का दाम भी नहीं मिल रहा है। कई जगहों पर किसानों ने रोटावेटर चलाए और प्याज की खड़ी फसल काट ली गई। किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार की नजर में प्याज उत्पादकों की पीड़ा का भी कोई औचित्य नहीं है।
सरकार और व्यापारी, किसानों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। किसानों को फसली कर्ज लेते समय जीएसटी भी देना होता है। राष्ट्रीयकृत बैंक और किसानों के अधिकार वाले जिला केंद्रीय बैंक भी हर साल फसल ऋण मंजूर करने के लिए किसानों से प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं। बैंक 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए 150 रुपये, 1 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 200 रुपये और उससे अधिक के ऋण के लिए 300 रुपये का प्रक्रिया शुल्क लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रणाली अलग है और ऋण स्वीकृति के लिए स्टाम्प शुल्क और निरीक्षण शुल्क लगाया जाता है। निरीक्षण शुल्क की राशि 708 रुपए निर्धारित है, जिसमें जीएसटी समाहित है।
लगातार विभिन्न प्रकार से सरकार को राजस्व प्रदान करने वाले किसान को कहीं भी बख्शा नहीं जाता है। माल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने के बाद व्यापारी ही किसानों से हर तरह का शुल्क वसूल करता है।
वह कृषि उत्पादों के दाम में भी उसे मात दे देता है। लूटपाट का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जिस किसान ने कर्ज लेने के लिए जीएसटी की गणना की है, उसे बाजार से सामान खरीदते समय भी हर वस्तु पर जीएसटी देना ही पडता है। कृषि सामग्री में भी कोई रियायत नहीं दी जाती। हालांकि फसली ऋण के लिए चुकाई जाने वाली जीएसटी की राशि न्यूनतम लगती है, लेकिन आर्थिक रूप से बर्बाद किसान के लिए यह जानलेवा हो जाती है। किसानों की अंधाधुंध लूट को रोकने के लिए एक बेहतर कृषि नीति लाने की जरूरत है। लेकिन न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष, इस बात पर ध्यान देने को तैयार है कि फसली कर्ज के बंटवारे में किसानों को लूटा जा रहा है!
राज्य सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है। किसान आत्महत्या को कम करने के लिए किसानों की न्यूनतम उत्पादन लागत को कम करने के लिए फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान 2018 में डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन की स्थापना की गई थी। उस समय 10 हजार हेक्टेयर के इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो केवल छह जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 4 साल में केवल 13 करोड़ यानी लगभग 10 फीसदी धनराशि ही दी गई थी। इसी बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार कृषि मुद्दों के प्रति उदासीन थी। अब एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब नई सरकार ने हाल ही में पेश बजट में कहा है कि डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा और 2.5 लाख हेक्टेयर को लाभ दिया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह जैविक किसानों को विशुद्ध रूप धोखा देने जैसा है। उस समय, 2018 से 2022 तक चार वर्षों के लिए घोषित जैविक मिशन पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च होने की उम्मीद थी। नवीनतम बजट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अब 3 वर्षों में केवल 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी केवल 1600 रुपये प्रति एकड़ यानी केवल 533 रुपये प्रति वर्ष खर्च होने की उम्मीद है। एक तरह से सरकार ने जैविक खेती करने की सिर्फ बात ही कही है। लेकिन मात्र ऐसी बातों से ही किसान जैविक खेती की ओर कैसे रुख करेंगे और आत्महत्याओं को कैसे रोकी जाएंगी?
चूंकि सरकार की नीति किसान विरोधी है, इसलिए अनावश्यक मुद्दों को हटाकर सरकार समय बर्बाद कर रही है, ताकि मीडिया या सभागृहों में किसानों के मुद्दे पर चर्चा ही न होने पाए! विदेशी शक्ति के प्रतीकों को खारिज करने में निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है। यह इतिहास है कि 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हुए स्वतंत्रता संग्राम के बाद न केवल कई शहरों के, बल्कि राज्यों के नाम भी बदले गए हैं।
स्वाभिमान और पहचान के लिए साम्राज्यवाद के नाम और प्रतीक बदलना स्वातंत्र्योत्तर काल में स्वाभाविक था। यह एक नए भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में सही कदम था। राष्ट्रीय पहचान की भावना थी। लेकिन अब वे शहर या स्थल राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जब शासक वर्ग, चाहे वह किसी भी दल का हो, के पास ताकत या क्षमता नहीं है, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति नहीं है, समाज और नागरिकों की समस्याओं को हल करने की बुद्धि नहीं है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कृषि में बीमारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की चुनौतियाँ, अर्थव्यवस्था को सहारा देने की चुनौतियाँ आदि… ऐसे सरल और भावनात्मक मुद्दों को बिना किसी कीमत के छुआ जाता है। तो अब यह समझना होगा कि किसानों को कब्र में डालने के कारण ही उसी समय औरंगजेब कब्र से बाहर निकालना पड़ा है! यहां असली शोकांतिका यही है कि जिन किसानों की धुलाई हो रही है, वे इन सब बातों पर इतनी मुस्तैदी से सोचते ही नहीं है!
– प्रकाश पोहरे
(संपादक– मराठी दैनिक देशोन्नति, हिन्दी दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नति)
संपर्क : 98225 93921
2prakashpohare@gmail.com